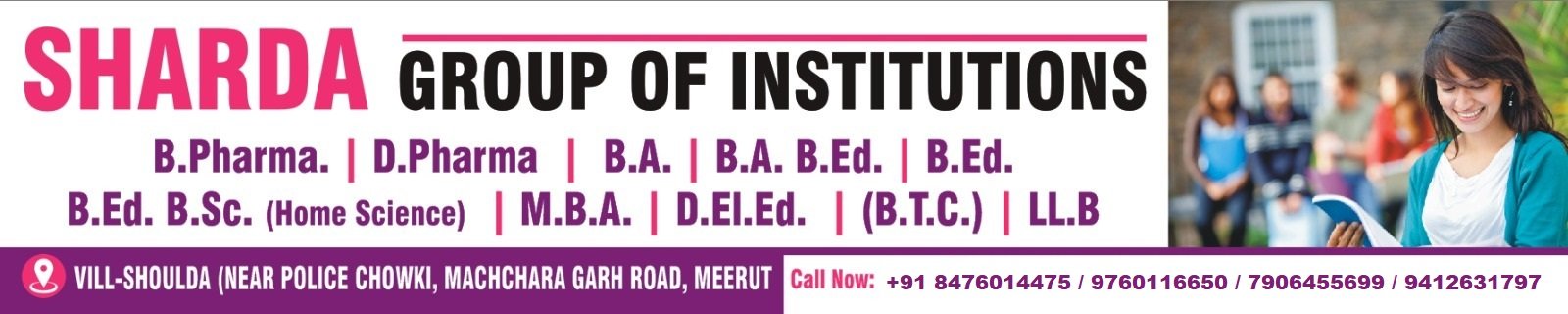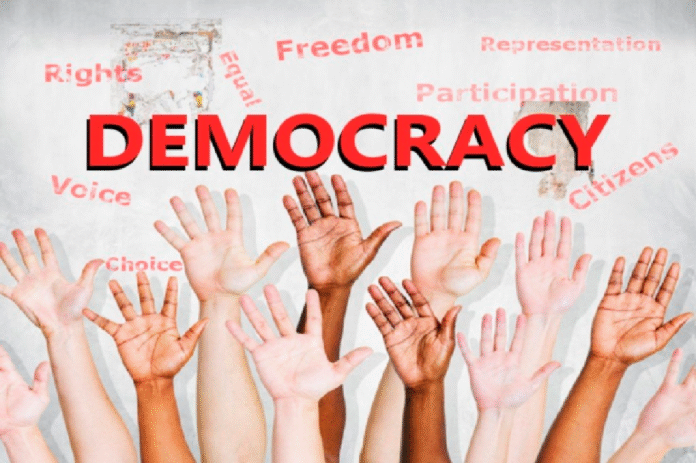मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: लोकतंत्र, नागरिकता और संविधान पर मंथन।

आदेश प्रधान एडवोकेट | भारत का लोकतंत्र अपनी नींव में जिस स्तंभ पर सबसे अधिक निर्भर है, वह है जनता की भागीदारी। यह भागीदारी चुनावों के माध्यम से सामने आती है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का उपयोग करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मतदाता सूची उस अधिकार का आधिकारिक रूप है जो तय करता है कि किसे यह हक़ मिलेगा और किसे नहीं। वर्ष 2025 के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व चुनाव आयोग ने इस सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया शुरू की, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक सुनवाई हुई।
चुनाव आयोग ने इस SIR को “आवश्यक प्रक्रिया” बताया जो मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट प्रविष्टियों, मृत व्यक्तियों और गैर-नागरिकों को हटाना अनिवार्य है ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। आयोग ने यह दलील दी कि यह अधिकार उसे संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 326 कहता है कि हर भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, उसे बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार है।

लेकिन इस प्रक्रिया पर विपक्ष, नागरिक समाज और कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल असंवैधानिक है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर भी चोट है। उनके अनुसार चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे सामान्य पहचान दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में अस्वीकार कर दिया है, जिससे विशेष रूप से गरीब, प्रवासी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय प्रभावित होंगे, जिनके पास सीमित दस्तावेज ही उपलब्ध हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि आयोग की यह मांग कि मतदाता को अपने माता-पिता के जन्मस्थान और जन्मतिथि का प्रमाण देना होगा, न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि इसके पीछे की मंशा भी संदेहास्पद है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ—न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची—ने इस प्रक्रिया पर कई तीखे प्रश्न पूछे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि यदि किसी नागरिक को सूची से हटाया जाता है, तो क्या वह चुनाव से पूर्व अपने मताधिकार को पुनः प्राप्त कर सकेगा? जस्टिस बागची ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सूची से हटाया जाता है, तो उसे अपील करनी होगी, प्रक्रिया से गुजरना होगा और तब तक चुनाव समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यही है कि उसे उस चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं मिलेगा, जो कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है।
एक अन्य अहम बिंदु यह था कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच करने का अधिकारी है या नहीं। आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग नागरिकता की जांच नहीं करता, बल्कि “संभाव्य प्रमाणों” के आधार पर यह सुनिश्चित करता है कि केवल नागरिक ही सूची में रहें। इस पर अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, बल्कि यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जब आप किसी व्यक्ति के दस्तावेजों को खारिज करते हैं और उसे सूची से हटाते हैं, तो यह कार्य वस्तुत: नागरिकता तय करने जैसा ही है।
चुनाव आयोग का यह दावा कि उसने बड़ी संख्या में BLOs, BLAs और स्वयंसेवकों को इस प्रक्रिया में लगाया है, याचिकाकर्ताओं के लिए पर्याप्त नहीं था। उनका कहना था कि बिहार की 8 करोड़ से अधिक की मतदाता जनसंख्या को इतने सीमित संसाधनों और सीमित समय में दस्तावेज़ इकट्ठा करने के लिए कहना न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि यह जानबूझकर योग्य मतदाताओं को वंचित करने की साजिश हो सकती है। यह बात विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, छात्रों और महिलाओं के लिए प्रासंगिक है जो या तो अपने घर से दूर रहते हैं या जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होते।
इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 325 (मतदान का अधिकार बिना भेदभाव के) की भी चर्चा हुई। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस प्रक्रिया से गरीब, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग disproportionate तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, जो संविधान के मूल सिद्धांतों का हनन है। इस बीच, विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधा सवाल बता दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही, बल्कि वह सरकार की एक शाखा की तरह कार्य कर रही है। उनका आरोप है कि यह SIR केवल कुछ वर्गों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने का साधन बन रहा है। वहीं, विपक्षी सांसदों जैसे महुआ मोइत्रा, मनोज झा, सुप्रिया सुले, डी. राजा, दीपंकर भट्टाचार्य आदि ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकने की मांग की गई है।
चुनाव आयोग ने यह भी तर्क दिया कि आधार कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस पर याचिकाकर्ताओं का उत्तर था कि यदि ऐसा है, तो फिर चुनाव आयोग Form 6 में आधार को अनिवार्य क्यों बना रहा है? यदि आधार नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसे अन्य सरकारी योजनाओं में नागरिक पहचान के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है? यह विरोधाभास केवल नागरिकों को भ्रमित करने और उन्हें प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास है। इस पूरी प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रवासी मजदूरों से जुड़ा है। RP Act की धारा 19 यह कहती है कि किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां वह मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहता है। लेकिन इसमें “अस्थायी अनुपस्थिति” को नागरिकता या मतदाता योग्यता से बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रवासी मजदूर अपने गांव-शहर लौटते रहते हैं, वे अपना नाम अपने गृह क्षेत्र में बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें सूची से हटाना उनके अधिकारों का हनन होगा।
यह भी उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने जनवरी 2023 में रिमोट वोटिंग (Remote Voting) की सुविधा की संभावना की बात की थी। लेकिन दो वर्षों में इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई। अब, जब बिहार जैसे राज्य में जहां लाखों लोग देश के अन्य हिस्सों में कार्यरत हैं, उनकी गैर-मौजूदगी में उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा—यह एक भयावह संभावना है जो लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंचा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में यह भी संकेत मिला कि न्यायालय चुनाव आयोग की मंशा पर नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया और समयबद्धता पर चिंतित है। कोर्ट का जोर इस बात पर रहा कि चुनाव से ठीक चार महीने पहले ऐसी प्रक्रिया शुरू करना, जब करोड़ों लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाना संभव नहीं, न केवल अनुचित है बल्कि यह संविधान के समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विरुद्ध भी है।
इस पूरी बहस में संविधान का अनुच्छेद 21 भी केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मतदान का अधिकार जीवन की गरिमा से जुड़ा है और किसी भी व्यक्ति को केवल दस्तावेजों के आधार पर वंचित करना न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि यह असंवैधानिक भी है।
न्यायमूर्ति बागची की टिप्पणी शायद इस सुनवाई का सारांश बन सकती है—”आप मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि गैर-नागरिक सूची में न रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप यह कार्य चुनाव से कुछ ही महीने पहले शुरू करते हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।” इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की मूलभूत आत्मा—समावेशिता, न्याय और समानता—की रक्षा के प्रति सजग है।
अब इस पूरे प्रकरण का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करता है, जिसकी सुनवाई 28 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। लेकिन जो बात स्पष्ट है वह यह कि लोकतंत्र केवल नियमों और प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से चलता है। यदि मतदाता सूची का पुनरीक्षण योग्य नागरिकों को वंचित करता है, तो वह केवल एक प्रशासनिक भूल नहीं बल्कि लोकतंत्र पर एक गहरा आघात होगा।
इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि वह अपने दृष्टिकोण को पुनः समीक्षा करे, विशेष रूप से उन वर्गों के संदर्भ में जो दस्तावेजीय रूप से वंचित हैं। आधार कार्ड जैसे व्यापक पहचान पत्रों को सहायक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और फॉर्म प्रक्रिया को सरल बनाकर, हेल्प डेस्क और मोबाइल सुविधा केंद्रों के माध्यम से लोगों की सहायता की जानी चाहिए। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं ताकि वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
यह मामला केवल बिहार की चुनावी प्रक्रिया का नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी ईमानदारी और समावेशिता की कसौटी भी है। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई केवल एक कानूनी कार्यवाही नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा का संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करना केवल अदालत का नहीं, बल्कि पूरे देश का कर्तव्य है।
नोट: संपादकीय पेज पर प्रकाशित किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना आवश्यक नही है ये लेखक के अपने विचार है।