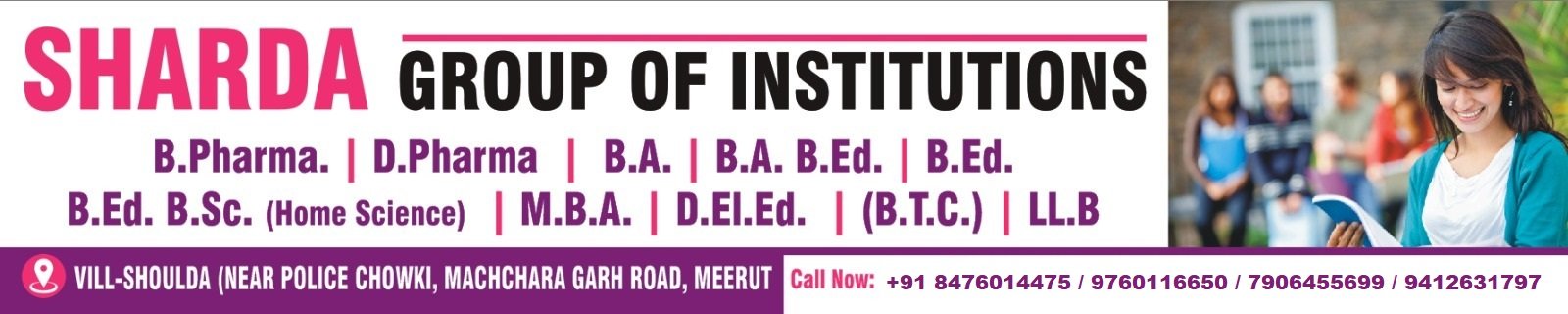घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल: जनता के लिए दोनों त्रासदी

आदेश प्रधान एडवोकेट | भारतीय संविधान का निर्माण इस भावभूमि पर हुआ था कि यह देश विधिक रूप से एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जहाँ प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी दी जाएगी। यह संविधान न केवल शासन की सीमाएं तय करता है, बल्कि नागरिकों को मौलिक अधिकारों का ऐसा सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है, जिसकी अनुपस्थिति किसी भी लोकतंत्र को निरर्थक बना सकती है। परंतु विडंबना देखिए कि इसी संविधान के दायरे में रहते हुए देश को न केवल घोषित आपातकाल का भयावह दौर देखना पड़ा, बल्कि आज एक ऐसा समय भी आया है, जब बिना किसी औपचारिक उद्घोषणा के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यह अघोषित आपातकाल है — विधिक परिधियों से बाहर नहीं, किंतु विधिक प्रक्रिया के भीतर उसकी आत्मा को खोखला कर देने वाली वह स्थिति जिसमें संविधान जीवित है परंतु मौलिक अधिकार मृतप्राय हैं।
घोषित आपातकाल भारत में 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्र की सुरक्षा को बाह्य आक्रमण या आंतरिक संकट से खतरा हो, तो राष्ट्रपति के परामर्श से प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक अस्थिरता और न्यायिक फैसले के बाद उत्पन्न स्थिति को आधार बनाते हुए देश में आंतरिक संकट की घोषणा कर दी। इसके परिणामस्वरूप नागरिकों के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा) तक को निलंबित कर दिया गया।
इस अवधि में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोके लगा दी गई। न्यायपालिका निष्क्रिय कर दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं को गैरकानूनी अधिनियमों के तहत वर्षों जेल में रखा गया। रेलवे कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल का दमन, जेपी आंदोलन पर बलप्रयोग और न्यायालयों में अधिकारों की समाप्ति — यह सब घोषित आपातकाल की वे घटनाएँ थीं, जो केवल शासन नहीं, बल्कि संवैधानिक भावना को कुचलने के रूप में दर्ज हैं।

परंतु वह आपातकाल घोषित था। जनता को पता था कि उनके अधिकार निलंबित हैं। अख़बारों की स्याही सूख गई थी, परंतु वह स्याही सिसकियों के रूप में पाठकों के मन तक पहुँचती थी। संघर्ष स्पष्ट था। सत्ता और नागरिक आमने-सामने खड़े थे।
अब स्थिति इससे भी अधिक भयावह है। आज आपातकाल की कोई घोषणा नहीं हुई है, अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु उस समस्त वातावरण को पुनर्जीवित कर दिया गया है जिसमें जनता मौन है, बुद्धिजीवी भयभीत हैं, पत्रकार सलाखों के भीतर हैं, न्याय में विलंब को न्याय मान लिया गया है और असहमति को राष्ट्रद्रोह के समकक्ष स्थापित कर दिया गया है।
आज भारत में विचार की स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा है। संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विधिक प्रतिबंधों के माध्यम से इस सीमा तक नियंत्रित कर दिया गया है कि नागरिक अपने ही देश में आत्म-सेंसरशिप की अवस्था में जीने को विवश हैं। भारत में (राजद्रोह), (धार्मिक वैमनस्य) और विशेष रूप से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम जैसे कठोर विधानों का प्रयोग स्वतंत्र पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों, शिक्षाविदों और छात्रों पर किया जा रहा है। छात्रों की आवाज को समाप्त करने के लिए छात्र संघ चुनाव को सरकारो द्वारा समाप्त कर दिया गया । हर आवाज को दबाने के तोर- तरीके अपनाए जाने लगे है ।
उदाहरण के रूप में पत्रकार को केवल इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि वह हाथरस कांड पर रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। उनके विरुद्ध यूएपीए के अंतर्गत आरोप लगाए गए और उन्हें बिना किसी ठोस प्रमाण के वर्षों तक जेल में रखा गया। पत्रकारिता को शासन के लिए आईना बनने के स्थान पर उसकी आलोचना के भय से काँपता हुआ दर्पण बना दिया गया है। जब प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो और वह स्वयं भय में जी रहा हो, तो समझा जा सकता है कि लोकतंत्र किस स्थिति में है। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है ।
भीमा-कोरेगांव प्रकरण में तो कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को बिना आरोप सिद्ध हुए जेल में रखा गया है। गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, प्रोफेसर हनी बाबू, वरवरा राव, और आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोग वर्षों से विचाराधीन कैदी बने हुए हैं। न्याय की प्रक्रिया इतनी धीमी और बोझिल है कि यह स्वयं ही एक दंड बन जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं माना है कि विचार की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूलाधार है, किंतु यही स्वतंत्रता अब राज्यसत्ता की दृष्टि में असुविधाजनक हो गई है ।
संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। इस अधिकार की व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में विस्तृत की है। मानवाधिकार के अंतर्गत गरिमामय जीवन, स्वतंत्र सोच, आस्था और असहमति का अधिकार, सब इसी अनुच्छेद की आत्मा में निहित हैं। किंतु जब एक पादरी फादर स्टैन स्वामी को वृद्धावस्था और बीमारी के बावजूद न्याय मिलने से पूर्व मृत्यु हो जाए, तो यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, यह संविधान की आत्मा का लहूलुहान हो जाना होता है।
आज देश की न्यायिक प्रणाली स्वयं प्रश्नों के के घेरे में है। ‘न्याय में विलंब न्याय का इनकार होता है’ यह सिद्धांत अब खोखला प्रतीत होता है। पत्रकार और लेखक को शिक्षाविद एवं छात्रों अभियुक्त बनाकर महीनों और वर्षों तक केवल विचाराधीन बनाकर रखा जाता है। आरोपपत्र दाखिल नहीं होता, सुनवाई प्रारंभ नहीं होती, और जमानत तक नहीं दी जाती। यह स्थिति लोकतंत्र के उस स्तंभ को कमजोर करती है जिसे विधायिका और कार्यपालिका के दमन से बचाने के लिए बनाया गया था। वह न्यायपालिका है ।
इस सन्नाटे में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर भी प्रश्नन उठते हैं। 1976 में घोषित आपातकाल के दौरान ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आपातकाल की अवधि में अनुच्छेद 21 तक लागू नहीं होता, और नागरिकों को जीवन व स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं है। यह निर्णय भारत के विधिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जाता है। उसी निर्णय में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना का अल्पमत निर्णय संविधान की आत्मा का आखिरी स्वर था। उन्होंने लिखा था – “जीवन और स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा के बिना केवल राज्य की दया पर नहीं छोड़ी जा सकती।” आज जब अघोषित आपातकाल में न्यायालयों की चुप्पी लंबी होती जा रही है, तब एक बार फिर वही आशंका गहराती दिखती है – क्या विधिक संस्थाएँ स्वेच्छाचार के सामने झुक चुकी हैं?
इस पूरे परिदृश्य में सत्ता और विपक्ष की भूमिका भी निरीक्षण की अपेक्षा रखती है। घोषित आपातकाल के समय विपक्ष एकजुट होकर जनता के साथ खड़ा हुआ था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, और अनेक राजनेताओं ने कारावास की यातना भोगी किंतु सत्ता के समक्ष झुके नहीं। उनके लिए लोकतंत्र केवल एक राजनैतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन का आदर्श था। उन्होंने संविधान की रक्षा को सर्वोपरि माना। वहीं आज की स्थिति में विपक्ष बिखरा हुआ है, और जनहित के मुद्दों पर उसका स्वर या तो मौन है या दबा हुआ है। अघोषित आपातकाल में स्वतंत्र पत्रकारिता भी मर चुकी है मजदूरों के छात्रों के किसानों के मुद्दे अब न्यूज चैनलों में दिखाई नही पड़ते है । सत्ता की हनक के नीचे एवं पत्रकारिता ने घुटने टेक दिए है। स्वतंत्र पत्रकार और विपक्ष के नेता ऐसे चैनल को गोदी मीडिया कहकर पुकारा जा रहा है। यह कमजोरी अघोषित आपातकाल की स्वीकृति जैसी प्रतीत होती है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण केवल विधिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संकट है। जब राष्ट्रवाद की परिभाषा सत्ता द्वारा नियंत्रित की जाने लगे, जब धार्मिक असहमति को अपराध मान लिया जाए, और जब नागरिकों के विचारों को ‘देशद्रोह’ से जोड़कर देखा जाए – तब संविधान केवल ग्रंथ बन जाता है और लोकतंत्र एक अभिनय। इस समय भारत जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वह केवल राजनीतिक संकट नहीं है, यह एक संवैधानिक पतन की ओर संकेत है।
डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी – “यदि संविधान अच्छा भी हो पर चलाने वाले लोग खराब हों, तो संविधान असफल हो जाएगा।” आज जब असहमति को दंडित किया जा रहा है, जब विचारधारात्मक बहस को राष्ट्रविरोध में परिवर्तित किया जा रहा है, और जब जनहित के लिए खड़े होने वालों को ‘आतंकी’ ठहराया जा रहा है – तब स्पष्ट हो जाता है कि संविधान की व्याख्या नहीं, उसका उद्देश्य ही विकृत किया जा रहा है।
घोषित आपातकाल में अत्याचार स्पष्ट थे, शत्रु परिभाषित था, दमन दिखता था। अघोषित आपातकाल की त्रासदी इससे भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ न तो घोषणा है, न स्पष्ट दमन – केवल नियंत्रण, भय और चुप्पी है। सच बोलने वाला सत्ता से सवाल करने वाला हर व्यक्ति सट्टा का शत्रु नजर आता है । यह दमन छाया की भाँति है – सब जगह है, परंतु कोई स्पष्ट आकार नहीं।
जनता के लिए घोषित और अघोषित – दोनों आपातकाल त्रासदी हैं। जनता तब भी पीस रही थी जनता आज भी पीस रही है । लोकतंत्र में भय का स्थान नहीं होता, किंतु वर्तमान भारत में भय ही व्यवस्था बनता जा रहा है। न्यायालय की भूमिका, मीडिया की निष्पक्षता, विपक्ष की सजगता, और नागरिकों की चेतना – यह चारों स्तंभ आज डगमगा रहे हैं। यही अघोषित आपातकाल की परिभाषा है – बिना कहे सब कुछ नियंत्रित करना है ।
अब आवश्यकता है उस लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की, जिसमें संविधान को केवल ग्रंथ नहीं, जीवंत सिद्धांत माना जाए। जहाँ विचार की हत्या को राष्ट्रद्रोह नहीं, राष्ट्र रक्षा समझा जाए। और जहाँ न्याय केवल निर्णय नहीं, नागरिक सम्मान का पर्याय बने। जब तक यह नहीं होगा, तब तक यह त्रासदी जारी रहेगी – भले ही घोषित न हो, परंतु हर नागरिक के मन में अंकित होती रहेगी।
नोट: संपादकीय पेज पर प्रकाशित किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना आवश्यक नही है ये लेखक के अपने विचार है।